यह ठंढ और गांव का घूरा
नया साल फिर भीषण ठंड का सौगात लेकर आया है। गांव के लोगों को इसका अंदाजा पहले से था। गत साल भी ठंड का आगमन देर से जनवरी में ही हुआ था।
नया साल फिर भीषण ठंड का सौगात लेकर आया है। गांव के लोगों को इसका अंदाजा पहले से था। गत साल भी ठंड का आगमन देर से जनवरी में ही हुआ था। फरवरी -मार्च से पछुवा हवा के साथ गर्मी की अपनी धमक शुरू हो गई थी। इसका असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। कृषि वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को मौसम में इस तरह के बदलाव का कारण मानते हैं। कुछ अंशों में वे सही भी हैं, किंतु समग्रता में नहीं। मैं जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध दोहन को मुख्य वजह मानता हूं। प्रकृति को भयानक रूप से नुकसान पहुंचा कर अपनी झोली भरने की प्रवृति पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। खैर, बात मैं जाड़े के दिनों में गांव में लगने वाले घूरे से शुरू की थी। तब जाड़े का मौसम कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता था।
आभिजात्य वर्ग आज जिसे अलाव कहते हैं, गांव-देहात में उसे घूरा कहा जाता है। तब घूरे की अपनी खास पहचान थी, अपना खास वर्गचरित्र था। वैसे गांव-टोले में प्रायः हर दरवाजे पर घूरा लगाया जाता था। कुछ घास-फूस जमा कर दिए, शाम में उसमें आग जला दी। घंटे-दो घंटे में उस आग की तपिश खत्म। कुछ दरबाजे पर विशेष रूप से घूरा लगाया जाता था। ऐसे घूरे में शाम से सुबह तक आग जलती रहती और लोग आग तापते हुए आपस मे गपशप भी करते थे। इस तरह के घूरा लगाने का तरीका भी थोड़ा अलग था। दरवाजे या मवेशियों के बथान में एक-डेढ फीट व्यास का और एक-डेड फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता था। शाम में उस गड्ढे में सूखा गोबर (कर्रा) या उपले का टुकड़ा रख कर उसे धान के भूसे से ढक दिया जाता। फिर उसके ऊपर सूखी पत्तिया खूब दबा-दबा कर रखी जाती थी। इससे दूसरे दिन सुबह तक आग बनी रहती थी। घूरे के पास लोगों को बैठने के लिए धान के पुआल से बना बिरुआ रखा जाता था। बिरुआ बनाने की भी अपनी कला थी।एक बार का बना बिरुआ दो-दो साल टिकता था। शाम ढलते ही घूरे में आग लगा दी जाती। टोले के जवान, बूढ़े -बुजुर्ग घूरे के पास जुटने लगते। खेती-पथारी, माल मवेशी, शादी-विवाह, जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू हो जाती थी। इस बीच पटना रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी सुनने के लिए घूरे के पास रेडियो रख दिया जाता था। आपस में लोग मजाक भी खूब करते। हाट- बाज़ार, तीर्थ भ्रमण और मेले के अनुभवों को साझा किया जाता था। चौपाल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद घूरे के निकट की बैठकी समाप्त होती थी। इसमें एक सामूहिकता का भाव था। गांव में सम्पन्न परिवारों के दरवाजे पर भी उनके नौकर-चाकर घूरे का इंतजाम करते। ऐसे लोग दूसरों के दरवाजे पर घूरा तापने नहीं जाते थे। उनके पास लकड़ियों की बहुतायत रहती थी इसलिए घूरे में सूखी लकड़ियों का ही उपयोग होता था। आस-पास कुर्सियां रखी जाती। उस पर बैठ कर लोग घूरे का आनन्द लेते थे। घूरा-घूरा में भी हैसियत के अनुसार फर्क होता है, यह मैं बचपन में ही जान लिया था। अब तो जाड़े में वैसा घूरा कहीं लगता नहीं। घूरे वाली सामूहिकता भी वक्त के प्रवाह में नष्ट हो गई।
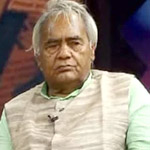
(ये लेखक के निजी विचार हैं। लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता/सटीकता के प्रति लेखक स्वयं जवाबदेह है। इसके लिए Swaraj Kh150abar उत्तरदायी नहीं है।)

