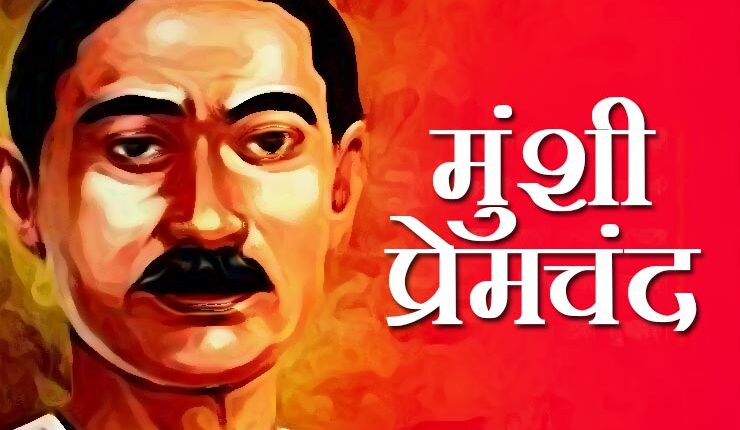ब्रह्मानन्द ठाकुर
आज विश्व विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती है। इस अवसर पर विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा इनकी जयंती बड़े पैमाने पर मनाने की परम्परा रही है। अबतक की परम्परा के अनुसार, किसी महापुरुष की जयंती मनाते हुए प्रायः यही कहा जाता रहा है कि हमें उनके गुणों और आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आदि! आदि!! ऐसा कहने वालों को शायद नहीं पता कि दुनिया का कोई भी महान से महान आदर्श चिरस्थाई नहीं होता, बल्कि देश, काल और परिस्थिति में परिवर्तन के साथ अतीत के तमाम आदर्श भी परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे में अतीत के महान से महान आदर्शों का वर्तमान में अंधानुकरण करने से लाभ के बदले हानि अधिक होती है। किसी भी घटना या वस्तुगत परिस्थिति पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से इस बात को समझ सकता है कि महान से महान प्रतिभाशाली व्यक्ति का चिंतन उसके स्थान, काल, परिस्थिति और भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर ही नहीं सकता। इसलिए मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर विचार करते समय इस प्रख्यात साहित्यकार की उन तमाम भौतिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना होगा, जिसमें उन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। तभी प्रेमचंद की कृतियों का सार तत्व प्राप्त हो सकेगा, जिसके सहारे शोषण, अत्याचार, सांस्कृतिक और नैतिक पतन के इस घुटन भरे माहौल से छुटकारा पाने के लिए देश की जनता को एक नई दिशा मिल सकेगी।
प्रेमचंद का रचनाकाल राजनीति, समाज नीति और कला के विभिन्न प्रयोगों तथा संघर्षों का काल है। देश में सामंती समाज व्यवस्था की जगह पूंजीवादी समाज व्यवस्था आकार ले रही थी, और भारत के गांवों में सामंतवाद के अवशेष कायम थे। लिहाजा इन दोनों के बीच परस्पर द्वंद्व की स्थिति थी। विदेशी शासक और देशी जमींदारों के शोषण से जनता कराह रही थी। समाज में नाना प्रकार की कुरीतियों, अंधविश्वास और धार्मिक वाह्य आडम्बर का बोलबाला था। युवा वर्ग अनुभव की अनेक छोटी-छोटी पगडंडियों से गुजर रहा था। नेतृत्व दिशाहीन था। विश्वास के नये आयाम बनते और मिटते जा रहे थे। आर्य समाज, हिंदु समाज, हरिजन उद्धार, सर्वोदय सभा जैसी सुधार समितियों का राजनीतिक मंच पर उदय हो चुका था। प्रेमचंद की तकरीबन 266 कहानियां तथा 10 उपन्यास तत्कालीन भारतीय समाज के उस संघर्षमय जिंदगी के गवाह हैं, जो उस समय की कठोर वास्तविकता से टकराते हुए, अपनी जीजिविषा के सहारे जी रहे थे। प्रेमचंद भारत के उन करोड़ों अशिक्षित, शोषित-पीडित जनता की जुबान थे, जिनके माध्यम से उनकी मूक वेदना बोलती थी। अपने कालजयी उपन्यास गोदान में उन्होंने न केवल इन समस्याओं को उठाया है, इसका समाधान भी सुझाया है। ग्रामीण जीवन के ‘गोबर तथा झुनियां’, ‘सिलिया’ और ‘मातादीन’ का प्रश्न आज भी हमारे सामाजिक जीवन को झकझोर रहे हैं। प्रेमचंद के समय ही तिलक-चंदन, कथा- प्रवचन, धर्म -संस्कार और पूजा-पाठ की मर्यादाएं झूठी पड़ चुकी थीं।
प्रेमचंद एक प्रगतिशील लेखक थे। उन्होंने मार्क्स और लेनिन के विचारों का अध्यन किया था। सोवियत समाजवादी क्रांति का उनपर प्रभाव था। कुछ यही कारण है कि उनकी रचनाओं में एक व्यावहारिक किस्म का समाजवाद दिखाई देता है। प्रेमचंद धन-धर्म और मान- प्रतिष्ठा से किसी भी कीमत पर समझौता का पक्षधर नहीं रहे। वे सही अर्थों में जनवादी लेखक थे। वे वैयक्तिक और सृजनात्मक दोनों क्षेत्रों में अंत तक केवल जनता के बने रहे। इस महान साहित्यकार को 1929 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर माल्कम हेली ने राय साहसी के खिताब से नवाजने की पेशकश की थी। इसके जवाब में प्रेमचंद ने जो लिखा वह आज के पुरस्कार के लिए लालायित साहित्यकारों की आंख खोलने वाला है। प्रेमचंद ने उनको लिखा था—- ‘तब मैं जनता का आदमी न रहकर एक पिट्ठू बन जाऊंगा। उसी तरह जैसे अन्य लोग हैं। अभी तक मेरा सारा काम जनता के लिए हुआ है। तब सरकार मुझसे जो लिखवाएगी, लिखना पड़ेगा।— जनता का तुच्छ सेवक हूं, अगर जनता की राय साहसी मिली तो सिर आंखों पर, गवर्न्मेंट की राय साहसी की इच्छा नहीं है।’ जाहिर है, आज की तरह तब भी जनता की इच्छा- आकांक्षाओं से अलग लेखकों का एक ‘सरकारी वर्ग’ भी था जिसे सिर्फ अपनी सुख-सुविधा और मान- सम्मान से मतलब था। प्रेमचंद साहित्यकारों के उस वर्ग में शामिल हो कर जनता को धोखा देना नहीं चाहते थे। इस महान साहित्यकार के जीवन का दूसरा पहलू यह है कि उन्हें ईश्वर या परम सत्ता जैसी किसी बात पर भरोसा बिल्कुल ही नहीं था। वे धर्म को समाज के विकास में बाधक मानते थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में तमाम पात्र धर्म का डटकर विरोध करते हैं। ‘प्रेम की वेदी’ कहानी में वे कहते हैं—‘आज दौलत जिस तरह आदमी का खून बहा रही है, उसी तरह, बल्कि उससे अधिक और ज्यादा बेदर्दी से धर्म ने आदमी का खून बहाने का काम किया है। दौलत इतनी कठोर नहीं होती, दौलत तो वहीं काम करती है, जिसकी उससे उम्मीद थी लेकिन धर्म तो प्रेम का संदेश लेकर आता है और काटता है आदमी का गला। वह मनुष्य के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर देती है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। आखिर सम्पूर्ण जगत में एक ही आत्मा तो है। धर्म का भेद क्या आत्मा की इस एकता को मिटा सकता है?’ तत्धाकालीन धार्मिक आडम्बर और क्रूरता प्रेमचंद से छिपा नहीं रहा। तभी तो सेवासदन का गजाधर कहता है, ‘तुमने उन लोगों के बड़े-बड़े तिलक-छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा मान लिया। आज तो धर्म धूर्तों का अड्डा बन गया है।’ आवश्यकता इस बात की है कि प्रेमचंद की कृतियों का वस्तुगत और वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए और आज के लेखन को वर्तमान सामाजिक- आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए प्रेमचंद की परम्परा को आगे बढ़ाया जाए।